Teachers Day Special 5 September 2025
Teachers Day Special 5 September 2025 : 5 सितंबर 2025, शिक्षक दिवस के इस खास मौके पर, आइए हम सब मिलकर एक गहन सवाल पर विचार करें: क्या भारत ‘विश्व गुरु’ बनने के लिए तैयार है? यह लेख सिर्फ शिक्षकों के सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी शिक्षा प्रणाली की नींव में छिपी चुनौतियों पर रोशनी डालता है। हम जानेंगे कि कैसे 21वीं सदी के कौशलों और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित ‘भारतीय शिक्षा सेवा’ (IES) की आवश्यकता है। साथ ही यह लेख शिक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारियों के एकाधिकार और नीति निर्माण में शिक्षकों की गैर-मौजूदगी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा करता है। इस शिक्षक दिवस, आइए शिक्षकों की वास्तविक भूमिका को पहचानें और भारत के उज्ज्वल भविष्य की राह तय करें।
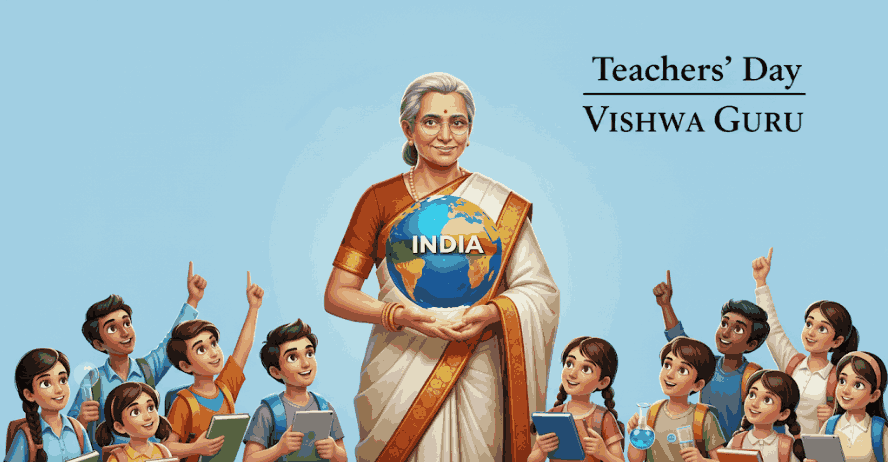
शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर, जब हम डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आदर्शों को याद करते हुए शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमारे मन में एक और विचार भी कौंधता है: क्या भारत वास्तव में ‘विश्व गुरु’ की अपनी प्राचीन उपाधि को फिर से हासिल कर पाएगा? यह प्रश्न केवल राजनीतिक या आर्थिक नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारी शिक्षा प्रणाली और उसमें शिक्षकों की स्थिति से है। यह लेख इसी गहन प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास है।
21वीं सदी के कौशल और हमारा शिक्षा तंत्र
आज हम 21वीं सदी के उस दौर में हैं, जहाँ केवल जानकारी रटने से काम नहीं चलेगा। इस युग में सफलता के लिए ‘4Cs’ – क्रिटिकल थिंकिंग (आलोचनात्मक सोच), क्रिएटिविटी (रचनात्मकता), कम्युनिकेशन (संचार) और कोलेबोरेशन (सहयोग) का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इन कौशलों के विकास की नींव विद्यालय और शिक्षक ही रखते हैं। लेकिन क्या हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली इन कौशलों को बढ़ावा दे रही है? विशेषकर, आलोचनात्मक सोच का महत्व सबसे अधिक है। एक छात्र को यह सिखाना कि वह किसी भी जानकारी को आँख बंद करके स्वीकार न करे, बल्कि उस पर सवाल उठाए, विश्लेषण करे और अपने निष्कर्ष पर पहुँचे, यही सही शिक्षा है। दुर्भाग्य से, हमारी प्रणाली में सवाल पूछने को अक्सर अनुशासनहीनता माना जाता है। जब तक हम इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे, तब तक हम विश्व स्तरीय प्रतिभा का निर्माण नहीं कर सकते।
भारतीय शिक्षा सेवा (IES) की आवश्यकता
जब देश की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए IAS, राजस्व के लिए IRS, वन के लिए IFS और पुलिस व्यवस्था के लिए IPS जैसी समर्पित और विशेषज्ञ सेवाएँ हैं, तो यह सोचना स्वाभाविक है कि इस देश की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नींव—शिक्षा—के लिए एक समर्पित भारतीय शिक्षा सेवा (IES) क्यों नहीं है? आज शिक्षा नीति और प्रबंधन का कार्य उन अधिकारियों के हाथों में है, जिनका विशेषज्ञता का क्षेत्र केवल प्रशासन है न कि शिक्षा। एक कुशल प्रशासक व्यवस्था को सुचारु रूप से चला सकता है, लेकिन एक शिक्षक की शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक समझ केवल एक शिक्षक ही रख सकता है। शिक्षा केवल एक विभाग नहीं है, यह एक जीवित, गतिशील प्रक्रिया है जिसे प्रबंधकों से कहीं अधिक शिक्षकों की विशेषज्ञता की आवश्यकता है। एक समर्पित IES का निर्माण शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता और जवाबदेही लाएगा, जिससे नीतियों का निर्माण जमीन पर काम करने वाले शिक्षकों के अनुभव के आधार पर हो सकेगा।
नीतियों में शिक्षकों की गैर-मौजूदगी
वर्तमान में भारतीय नीति और व्यवस्था विभिन्न सेवाओं द्वारा चलाई जाती है लेकिन इसमें स्कूल और कॉलेज शिक्षा क्षेत्र का उचित प्रतिनिधित्व न के बराबर है। शिक्षा व्यवस्था को चलाने वाले उच्च अधिकारी अक्सर शिक्षकों से दूर रहते हैं, जबकि शिक्षकों की भूमिका केवल कक्षा तक सीमित नहीं है। वे छात्रों के चरित्र, सोच और दृष्टिकोण को गढ़ते हैं। वे समाज के निर्माता और संहारक होते हैं। किसी भी राष्ट्र के विकास में उनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब तक शिक्षकों को नीति-निर्माण की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता, तब तक बनाई गई नीतियाँ केवल कागजी कार्रवाई बनकर रह जाती हैं। उन्हें भारतीय व्यवस्था में वह स्थान मिलना चाहिए जिसके वे वास्तव में हकदार हैं।
शिक्षक: शिक्षा प्रणाली के असली पायलट
यह प्रश्न आज हर जगह गूँज रहा है कि क्या भारत सच में ‘विश्व गुरु’ बनेगा? लेकिन जब तक हमारे शिक्षकों को व्यवस्था में प्रमुख स्थान नहीं मिलेगा, तब तक इस प्रश्न का उत्तर संदेह से भरा रहेगा। शिक्षक शिक्षा प्रणाली के पायलट हैं लेकिन आज उच्च अधिकारी खुद को ही पायलट मान बैठे हैं। वे शिक्षकों को केवल निर्देश और आदेश देते हैं कि उन्हें कब, कहाँ और कैसे काम करना है। पायलट को अपने विमान को सुरक्षित रूप से उड़ाने के लिए परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक उसी तरह शिक्षकों को भी कक्षा में अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए स्वायत्तता और सम्मान मिलना चाहिए। जब शिक्षक को केवल एक आज्ञाकारी कर्मचारी की तरह देखा जाता है, तो उसकी रचनात्मकता और पढ़ाने का जुनून खत्म हो जाता है, जिसका सीधा असर छात्रों पर पड़ता है।
प्रशासनिक अधिकारियों का एकाधिकार: मध्य प्रदेश का उदाहरण
मध्य प्रदेश में शिक्षा का उच्च विभाग DPI (लोक शिक्षण संचालनालय), MPBSE (माध्यमिक शिक्षा मंडल) और RSK (राज्य शिक्षा केंद्र) जैसे संगठनों द्वारा चलाया जाता है। इन सभी संस्थाओं के प्रमुख पद अक्सर IAS अधिकारियों के पास होते हैं। हालाँकि ये अधिकारी अपने क्षेत्र में अत्यंत कुशल होते हैं लेकिन उन्हें शिक्षण विधियों, शैक्षणिक प्रदर्शन प्रथाओं या शिक्षा मनोविज्ञान की कोई जानकारी नहीं होती। उनका ध्यान केवल प्रशासनिक पहलुओं पर होता है जैसे फंड आवंटन, रिपोर्टिंग और नियमों का पालन। वे यह नहीं समझ पाते कि एक कक्षा के अंदर छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ क्या हैं या सबसे प्रभावी शिक्षण तकनीक क्या हो सकती है। यह प्रशासनिक एकाधिकार शिक्षा की गुणवत्ता में एक बड़ी बाधा बन जाता है।
डिजिटल अव्यवस्था और प्रशासनिक बोझ
आज के डिजिटल युग में यह कल्पना करना कठिन है कि DPI की कोई व्यवस्थित वेबसाइट नहीं है। यहाँ तक कि सरकारी पत्र भी व्हाट्सएप जैसे निजी सोशल मीडिया माध्यमों से प्रसारित किए जाते हैं। यह न केवल अव्यवसायिक है, बल्कि इससे महत्वपूर्ण जानकारी के खो जाने और गलत सूचना के फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। अधिकांश सरकारी वेबसाइटों का उपयोग केवल उन्हीं आदेशों को प्रसारित करने के लिए होता है जो अधिकारी चाहते हैं। आश्चर्यजनक रूप से 90 प्रतिशत पत्र प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित होते हैं और शैक्षणिक कार्यों के लिए कोई मार्गदर्शन या निर्देश जारी नहीं किए जाते। शैक्षणिक संसाधन विभिन्न वेबसाइटों पर बिखरे हुए हैं और उन्हें एक जगह पर लाने में अधिकारियों की कोई रुचि नहीं दिखती। इस अव्यवस्था से शिक्षकों को सही जानकारी और सामग्री खोजने में बहुत कठिनाई होती है, जिससे उनका समय बर्बाद होता है और शैक्षणिक कार्यों पर से ध्यान हटता है।
शैक्षणिक जिम्मेदारी का अभाव
जब भी कोई नई योजना या तकनीक शुरू की जाती है, तो उसे लागू करने और सफल बनाने की जिम्मेदारी केवल शिक्षकों पर डाल दी जाती है। शिक्षक कार्यशालाओं और प्रशिक्षण में भाग लेते हैं और फिर खुद ही छात्रों के साथ इन नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं। दुर्भाग्य से कोई भी उच्च अधिकारी इन शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता या यह सुनिश्चित करने के लिए मैदान में नहीं उतरता कि ये योजनाएँ प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं या नहीं। शिक्षा व्यवस्था में यह ऊपर से नीचे की तरफ बहने वाला बोझ है, जहाँ शिक्षक केवल आज्ञाकारी कार्यकर्ता बनकर रह जाते हैं।
जेनरेशन गैप और पाठ्यक्रम का संकट
सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब भी कोई शिक्षा नीति या पाठ्यक्रम बनाया जाता है, तो उसमें सक्रिय शिक्षकों की उचित भागीदारी नहीं होती। स्कूल का पाठ्यक्रम अक्सर कॉलेज के शिक्षकों और सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि कॉलेज का पाठ्यक्रम सेवानिवृत्त प्रोफेसरों द्वारा। इसका परिणाम यह होता है कि पाठ्यक्रम अक्सर पुराना और अप्रासंगिक होता है। आज के छात्र 21वीं सदी की पीढ़ी हैं, जो डिजिटल उपकरणों और सूचना के विस्फोट के साथ बड़े हुए हैं। वहीं हमारे अधिकांश शिक्षक 20वीं सदी की सोच और तरीकों से जुड़े हैं। इस विशाल जेनरेशन गैप को कम करने के लिए पाठ्यक्रम में लगातार सुधार और वर्तमान में काम कर रहे शिक्षकों को इसमें शामिल करना अत्यंत आवश्यक है।
निष्कर्ष
शिक्षक दिवस केवल शिक्षकों का सम्मान करने का दिन नहीं है बल्कि यह हमारे शिक्षा तंत्र पर विचार करने का भी दिन है। अगर हम सच में भारत को ‘विश्व गुरु’ बनाना चाहते हैं, तो हमें शिक्षकों को वह सम्मान, अधिकार और स्वायत्तता देनी होगी जिसके वे हकदार हैं। हमें एक ऐसा तंत्र बनाना होगा जहाँ शैक्षणिक विशेषज्ञता को प्रशासनिक प्रबंधन से ऊपर रखा जाए, जहाँ शिक्षकों की आवाज सुनी जाए और जहाँ वे केवल आदेशों का पालन करने वाले नहीं बल्कि बदलाव के वास्तुकार बनें। जब तक ऐसा नहीं होता, “विश्व गुरु” का सपना एक अधूरा ख्वाब ही रहेगा।
1 thought on “क्या भारत विश्व गुरु बनेगा? शिक्षक ही हैं इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब Teachers Day Special 5 September 2025”